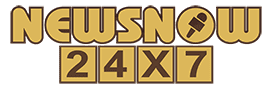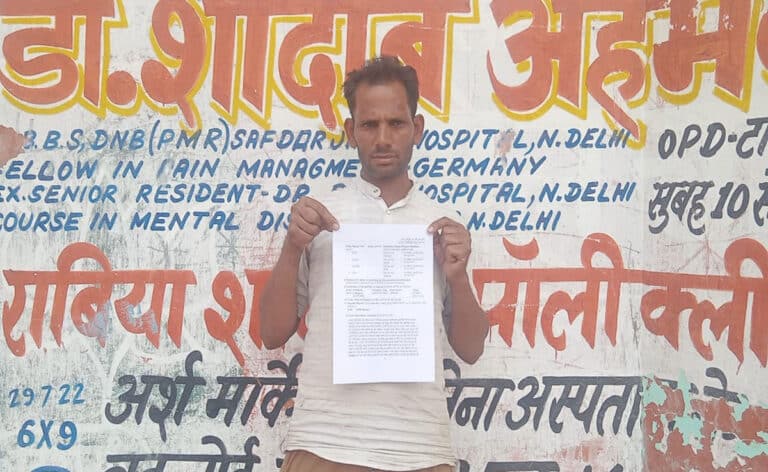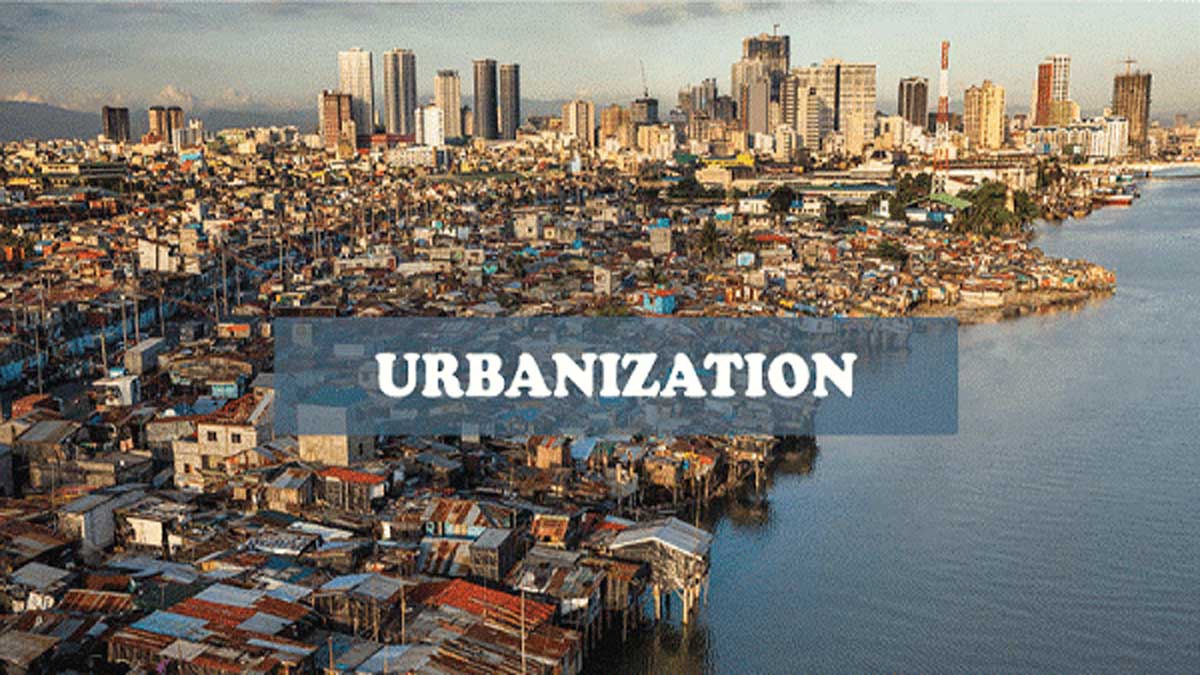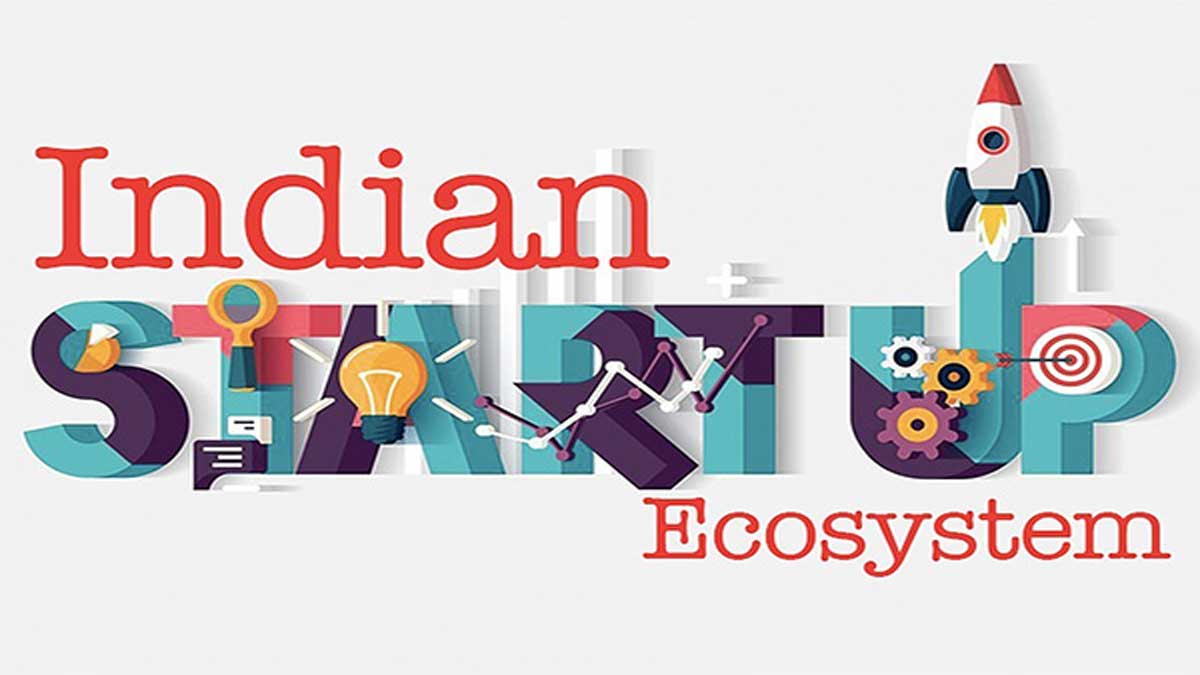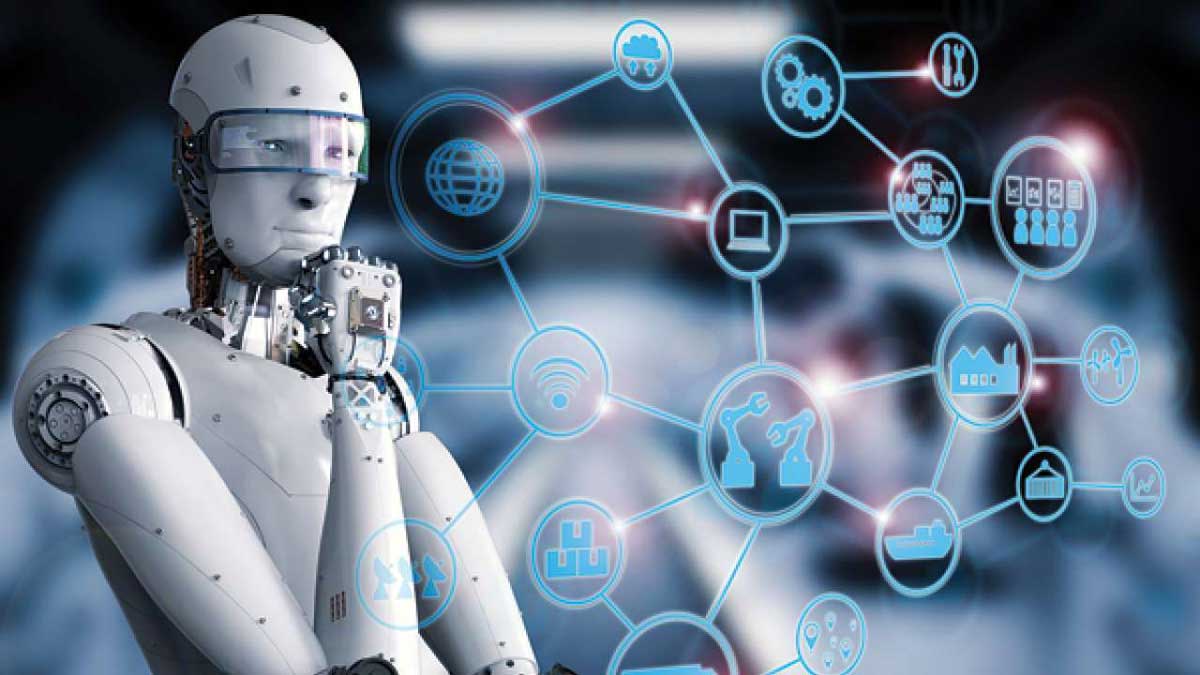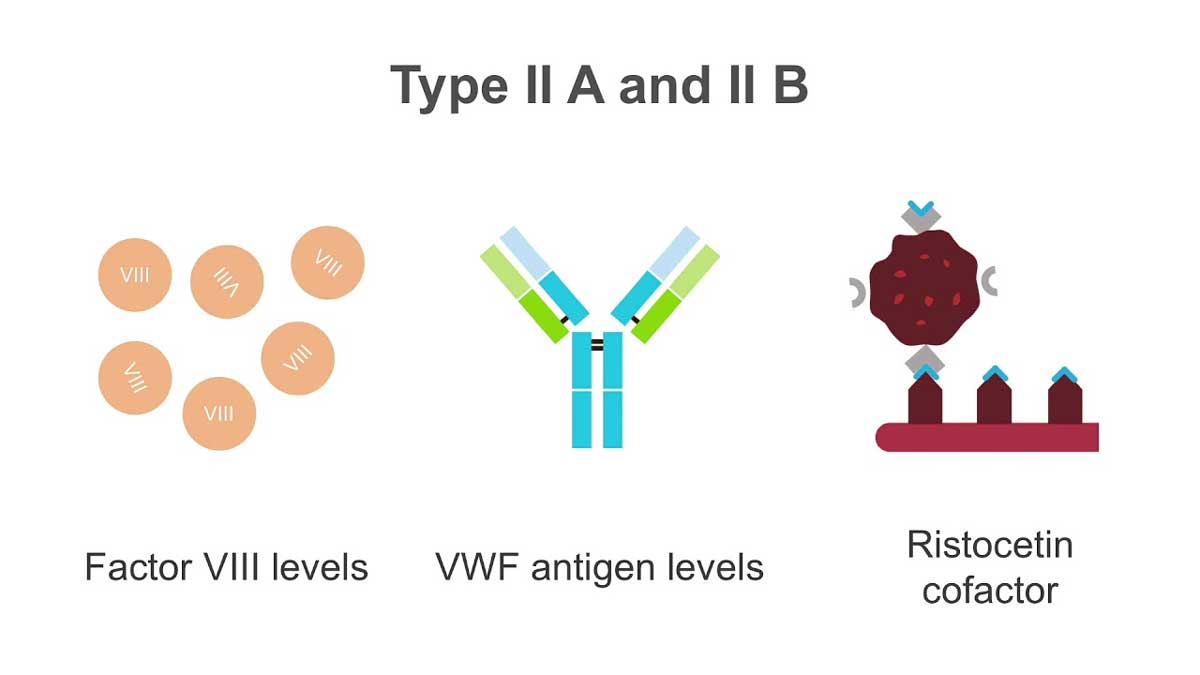बॉलीवुड की यंग और ग्लैमरस एक्ट्रेस Ananya Pandey इन दिनों हर तरफ छाई हुई हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म ‘केसरी 2’ की चारों ओर चर्चा हो रही है, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने एक ऐसा खिताब अपने नाम कर लिया है, जो अब तक किसी भी भारतीय महिला एक्ट्रेस को नहीं मिला था। जी हां, Ananya Pandey एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर फॉरेन फैशन ब्रांड की पहली भारतीय महिला एंबेसडर बन गई हैं। इस उपलब्धि ने उन्हें बॉलीवुड की ग्लोबल डिवा की कैटेगरी में खड़ा कर दिया है।
सामग्री की तालिका
कौन सा है ये विदेशी ब्रांड?
Ananya Pandey को जो ब्रांड एंबेसडर का खिताब मिला है, वो कोई छोटा-मोटा नाम नहीं है। ये है ‘VERSACE’ – दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और हाई-फैशन लग्जरी ब्रांड्स में से एक। वर्साचे फैशन की दुनिया में एलिगेंस, क्लास और ग्लैमर का दूसरा नाम है। मेडोना, लेडी गागा, जेनिफर लोपेज और गिगी हदीद जैसी हॉलीवुड हस्तियां इसके लिए रैंप वॉक कर चुकी हैं। और अब इस लिस्ट में Ananya Pandey का नाम भी जुड़ गया है।
पहली भारतीय महिला एंबेसडर बनने का गौरव

यह पहली बार है जब वर्साचे ने किसी भारतीय महिला को अपने ब्रांड एंबेसडर के तौर पर चुना है। इससे पहले कुछ भारतीय पुरुष मॉडल्स को वर्साचे के लिए काम करने का मौका मिला था, लेकिन एक फेस ऑफ द ब्रांड बनने का सम्मान पहली बार किसी इंडियन एक्ट्रेस को मिला है।
अनन्या का चयन इस बात को साबित करता है कि अब भारतीय टैलेंट को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर पहले से कहीं ज्यादा सम्मान और पहचान मिल रही है। और यह भी कि अनन्या सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं, बल्कि अब वह ग्लोबल फेम की ओर तेजी से बढ़ रही हैं।
वर्साचे के लिए पहली शूटिंग
इस उपलब्धि के बाद अनन्या ने वर्साचे के लिए अपना पहला फोटोशूट भी पूरा कर लिया है। ब्लैक और गोल्ड शेड्स में उनके लुक ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। उन्होंने जो ड्रेस पहनी है, वह वर्साचे की 2025 स्प्रिंग कलेक्शन से है – जो अभी तक किसी भी पब्लिक इवेंट में नहीं दिखी थी।
Ananya Pandey: उनकी तस्वीरों पर इंटरनेशनल फैशन क्रिटिक्स ने भी रिएक्ट किया है और अनन्या के स्टाइल और एटीट्यूड की जमकर तारीफ की है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीरों पर 24 घंटे के अंदर 10 लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं।
वर्साचे ने क्यों चुनी अनन्या?
अब सवाल ये है कि वर्साचे जैसे इंटरनेशनल ब्रांड ने Ananya Pandey को क्यों चुना? इसका जवाब छिपा है अनन्या की पर्सनालिटी में – यूथफुलनेस, कंफिडेंस, एक्सपेरिमेंटल स्टाइल और फ्रेश फेस की वजह से अनन्या ने फैशन इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान बना ली है।
अनन्या ना सिर्फ फिल्मों में एक्टिव हैं, बल्कि वे सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 25 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसके साथ ही वे अक्सर इंटरनेशनल इवेंट्स – जैसे कांस फिल्म फेस्टिवल और मिलान फैशन वीक में भी नजर आती रही हैं। इन सबने मिलकर उन्हें एक परफेक्ट चॉइस बना दिया।
‘केसरी 2’ की रिलीज से पहले बड़ी कामयाबी
Ananya Pandey: ‘केसरी 2‘ के ट्रेलर ने पहले ही सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है। फिल्म में अनन्या का रोल एक बहादुर रिपोर्टर का है जो सीमावर्ती इलाके में रिपोर्टिंग करती है और भारतीय जवानों की जिंदगी से रूबरू होती है।

फिल्म में अक्षय कुमार और अनन्या की जोड़ी को पहली बार बड़े पर्दे पर देखा जाएगा। लेकिन इससे पहले ही वर्साचे की एंबेसडर बनकर अनन्या ने अपने करियर को एक नया आयाम दे दिया है।
बी-टाउन में मची हलचल
जैसे ही वर्साचे के साथ Ananya Pandey की डील की खबर आई, बॉलीवुड इंडस्ट्री में हलचल मच गई। कई सेलेब्स ने उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दी –
- करण जौहर ने लिखा: “Proud of you girl! From Student of the Year to Global Icon – what a journey!”
- शिल्पा शेट्टी ने कमेंट किया: “You go girl! You are making India proud.”
- जाह्नवी कपूर और सारा अली खान ने भी इंस्टा स्टोरीज़ पर अनन्या की फोटो शेयर कर उन्हें बधाई दी।
Ananya Pandey का फिल्मी सफर: बॉलीवुड का नया उभरता सितारा
एक्ट्रेसेज़ की रेस में सबसे आगे
जहां कई एक्ट्रेसेज़ अब भी भारतीय ब्रांड्स के लिए शूट कर रही हैं, अनन्या ने इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम दर्ज कराकर ये साबित कर दिया है कि वो ग्लोबल स्टाइल आइकन बनने की काबिलियत रखती हैं। प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण भले ही हॉलीवुड में पैर जमा चुकी हों, लेकिन फैशन की दुनिया में अनन्या की यह शुरुआत उन्हें एक नया मुकाम दिला सकती है।
खुद Ananya Pandey ने क्या कहा?
इस मौके पर Ananya Pandey ने कहा –

“मैं बेहद सम्मानित महसूस कर रही हूं कि मुझे वर्साचे जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड का हिस्सा बनने का मौका मिला। यह सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक सपना है जो साकार हुआ है। भारत का प्रतिनिधित्व करना और दुनिया को दिखाना कि हमारे पास कितनी प्रतिभा है – इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती।”
ब्रांड्स की नजर अब अनन्या पर
अब जब वर्साचे जैसे बड़े ब्रांड ने अनन्या पर भरोसा जताया है, तो उम्मीद है कि और भी इंटरनेशनल ब्रांड्स उन्हें साइन करने के लिए आगे आएंगे। फैशन और ब्यूटी ब्रांड्स की दुनिया में ये नाम सामने आ सकते हैं:
- Dior
- Louis Vuitton
- Chanel
- Fenty Beauty
अनन्या का स्टाइल गेम
अगर आपने अनन्या का इंस्टाग्राम फीड देखा हो, तो आप जानते होंगे कि वह फैशन के साथ खूब एक्सपेरिमेंट करती हैं। मिनी ड्रेस हो या ट्रेडिशनल साड़ी, जॉगर्स हों या हाई फैशन गाउन – अनन्या हर लुक को कैरी करने का हुनर रखती हैं। इसलिए ही शायद वर्साचे ने उन्हें चुना – क्योंकि वह फैशन को सिर्फ पहनती नहीं, बल्कि जीती हैं।
Ananya Pandey का सबसे स्टाइलिश लहंगा लुक
क्या बदल जाएगा अब?
अब जब अनन्या वर्साचे की ब्रांड एंबेसडर बन गई हैं, तो उनका करियर सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहेगा। उन्हें जल्द ही इंटरनेशनल रैंप वॉक करते और फैशन वीक के रेड कार्पेट पर स्पॉट किया जा सकता है।
हो सकता है आने वाले समय में उन्हें किसी हॉलीवुड प्रोजेक्ट में भी देखा जाए। प्रियंका चोपड़ा के बाद अगर कोई यंग एक्ट्रेस है जो इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम रोशन कर सकती है, तो वो है – Ananya Pandey।
निष्कर्ष
‘केसरी 2’ की रिलीज से पहले Ananya Pandey ने वर्साचे की ब्रांड एंबेसडर बनकर जो उपलब्धि हासिल की है, वो न सिर्फ उनकी पर्सनल सक्सेस है बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का मौका है। फैशन की दुनिया में यह कदम उनके लिए एक नया दरवाजा खोल सकता है। अब देखना ये होगा कि ‘केसरी 2’ में उनकी परफॉर्मेंस इस ग्लोबल पहचान को और मजबूती देती है या नहीं। लेकिन इतना तय है कि Ananya Pandey का सितारा अब सिर्फ बॉलीवुड नहीं, बल्कि इंटरनेशनल स्काई में चमकने वाला है।
अन्य ख़बरों के लिए यहाँ क्लिक करें